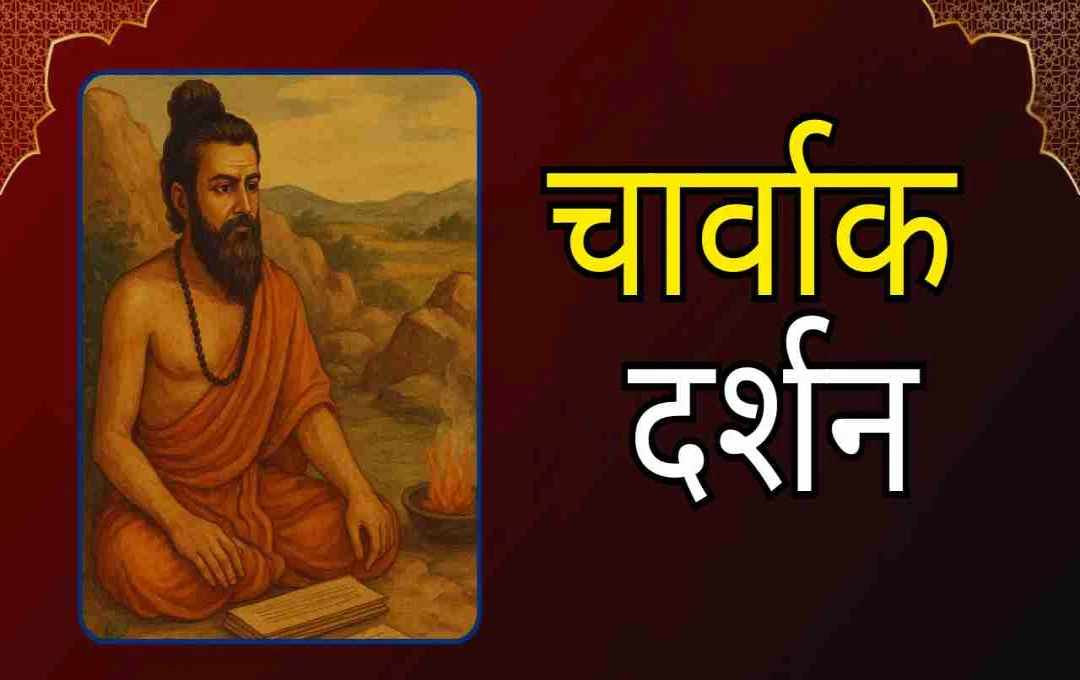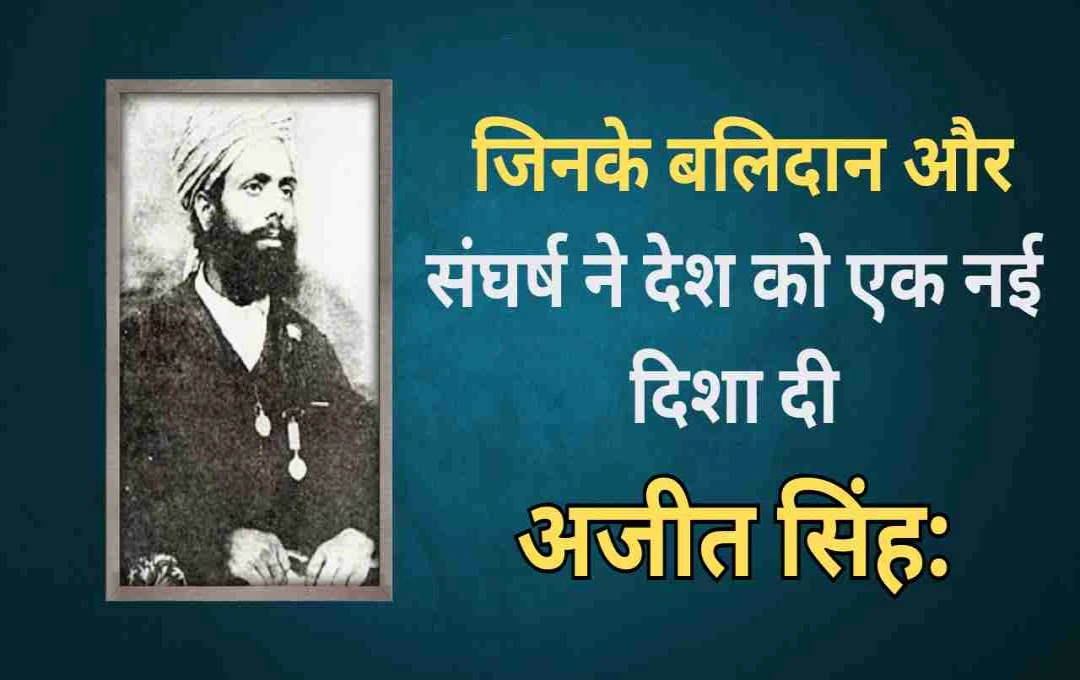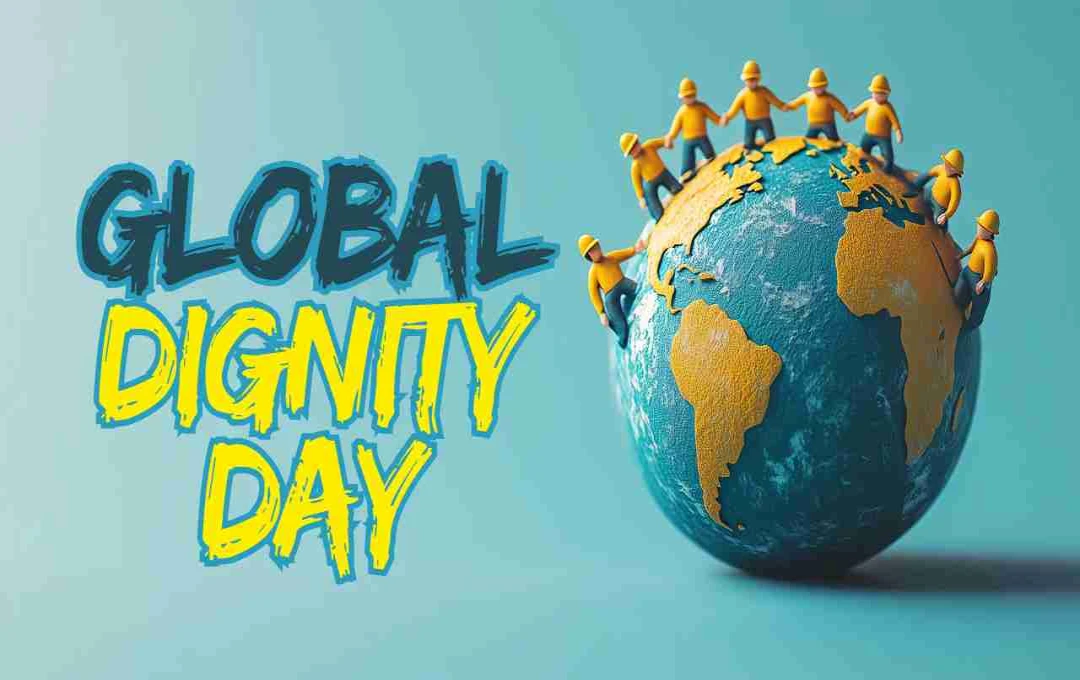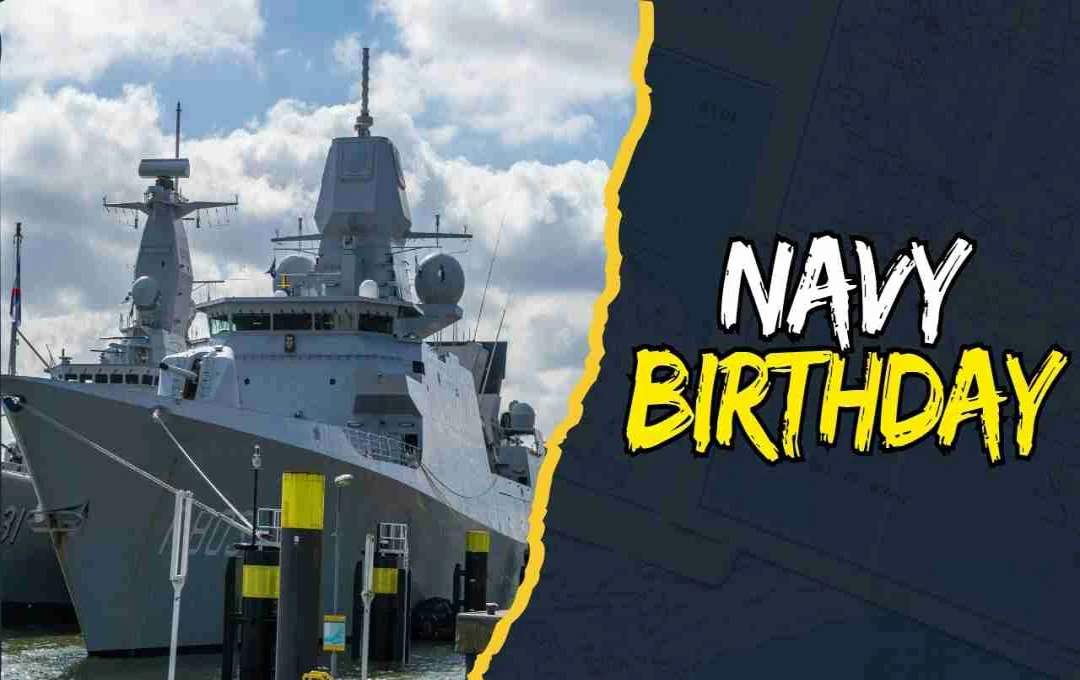प्राचीन भारतीय नास्तिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण, जो प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक सुख को सर्वोच्च मानता है। यह दर्शन ईश्वर, आत्मा, मोक्ष और परलोक की अवधारणाओं को अस्वीकार करता है और जीवन को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखता है।
Charvaka Philosophy: भारतीय दर्शनशास्त्र की समृद्ध परंपरा में चार्वाक दर्शन एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह दर्शन अपने नास्तिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। चार्वाक दर्शन अन्य आस्तिक या वेदसिद्ध दर्शनशास्त्रों से भिन्न है, क्योंकि यह केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को मान्यता देता है और किसी भी प्रकार की पारलौकिक सत्ता, ईश्वर, आत्मा या मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता। इसे प्राचीन काल में ‘लोकायत दर्शन’ के नाम से भी जाना जाता था।
चार्वाक दर्शन का इतिहास
चार्वाक दर्शन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। इसका प्रत्यक्ष ग्रंथ—बृहस्पति सूत्र (लगभग 600 ईसा पूर्व)—आज उपलब्ध नहीं है। अधिकांश प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथ खो चुके हैं, जिससे इसका अध्ययन केवल अन्य ग्रंथों और ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से ही संभव हुआ है।
चार्वाक दर्शन के प्रणेता के रूप में दो प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है—अजित केशकंबली और बृहस्पति। अजित केशकंबली को इसके प्रारंभिक प्रवर्तक के रूप में माना जाता है, जबकि बृहस्पति को इसे व्यवस्थित करने और प्रचारित करने वाला प्रमुख शिक्षक माना गया।
चार्वाक दर्शन का मूल उद्देश्य जीवन को यथार्थ और प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर समझना था। यह दर्शन वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित पारलौकिक और अलौकिक तत्त्वों को स्वीकार नहीं करता। इसलिए इसे वेदबाह्य दर्शन कहा गया। वेदबाह्य दर्शन के अंतर्गत छह प्रमुख दृष्टिकोण आते हैं—चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक और आर्हत (जैन)। इनमें चार्वाक दृष्टिकोण अपने साक्षातवादी (प्रत्यक्षवादी) दृष्टिकोण और नास्तिकता के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
चार्वाक दर्शन का नाम और अर्थ
चार्वाक शब्द की उत्पत्ति में विभिन्न मत हैं। प्रचलित धारणा यह है कि ‘चार्वाक’ का संबंध ‘चर्वण’ या ‘खाना-पीना’ से है। इसके अनुसार, यह दर्शन जीवन में भौतिक सुख और आनन्द को प्रधान मानता है। ग्रंथ ‘गुणरत्न’ के अनुसार, चार्वाक दर्शन का अर्थ है—परमेश्वर, वेद, पुण्य-पाप, स्वर्ग-नरक, आत्मा और मोक्ष जैसे सिद्धांतों का परित्याग करना।
सामान्य जीवन के दृष्टिकोण से चार्वाक दर्शन को लोकप्रिय और सहज दर्शन माना जाता है। इसके अनुयायी कहते हैं कि जीवन में सुख ही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए और इसके लिए मानव को यथासंभव अपने इन्द्रियों और शरीर की तृप्ति प्राप्त करनी चाहिए।
चार्वाक का भौतिकवादी तत्त्वमीमांसा
चार्वाक दर्शन के अनुसार, सृष्टि केवल चार महाभूतों—पृथ्वी, जल, अग्नि (तेज) और वायु—से बनी है। इनके विशेष संयोजन से ही शरीर और चेतनता उत्पन्न होती है। आत्मा नामक कोई स्वतंत्र तत्त्व नहीं है। यह भूतचैतन्यवाद कहलाता है।
चार्वाकों के अनुसार, जैसे गुड़ और तंदुल के संयोजन से मद्य उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चार महाभूतों के संयोजन से चेतनता उत्पन्न होती है। जब शरीर का विनाश होता है, तो चेतनता भी समाप्त हो जाती है। इस दृष्टिकोण को देहात्मवाद कहा जाता है।
चार्वाक का नास्तिक और निरीश्वरवादी दृष्टिकोण
चार्वाक दर्शन में ईश्वर और परलोक का अस्तित्व नहीं माना गया। उनका तर्क है कि यदि ईश्वर और परलोक का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, तो उनका अस्तित्व केवल अनुमान और कल्पना है, जिसे प्रमाण नहीं माना जा सकता।
चार्वाकों का यह भी मत है कि व्याप्ति और अनुमान आधारित ज्ञान असत्य और संदिग्ध है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि अज्ञात कारण से पेड़ पर पक्षियों का कोलाहल होगा, तो यह केवल संभाव्यता है। प्रत्यक्ष अनुभव ही ज्ञान का वास्तविक स्रोत है।
इस दृष्टिकोण से चार्वाक दर्शन में धर्म, पुण्य-पाप, स्वर्ग, नरक आदि की अवधारणाएँ निरर्थक और अप्रासंगिक मानी गई हैं।
आत्मा और चेतनता का सिद्धांत
चार्वाक दर्शन आत्मा को पृथक् तत्त्व नहीं मानता। उनके अनुसार शरीर और आत्मा एक ही हैं। चेतनता शरीर का गुण है। इस दृष्टिकोण को सिद्ध करने के तीन तरीके बताए गए हैं—तर्क, अनुभव और आयुर्वेद शास्त्र:
- तर्क: शरीर के रहते चेतनता होती है, शरीर नष्ट होने पर चेतनता समाप्त हो जाती है। अतः चेतनता शरीर का गुण है।
- अनुभव: हम अपने अनुभव से महसूस करते हैं कि हमारी स्थूलता, दुर्बलता और रंग आदि हमारे शरीर के गुण हैं। इसलिए आत्मा केवल शरीर का ही गुण है।
- आयुर्वेद शास्त्र: जैसे विभिन्न पदार्थों के सम्मिश्रण से नई वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, वैसे ही चार महाभूतों के संयोजन से चेतनता उत्पन्न होती है।
इस प्रकार चार्वाकों के अनुसार मृत्यु ही मोक्ष है, क्योंकि मृत शरीर किसी भी प्रकार का अनुभव नहीं करता।
चार्वाक का ज्ञानमीमांसा
चार्वाक दर्शन में ज्ञान का स्रोत केवल प्रत्यक्ष अनुभव है। यह दर्शन अन्य प्रमाणों—जैसे अनुमान, उपमा, शब्द या आप्त वचन—को ज्ञान का प्रमाण नहीं मानता।
उदाहरण के लिए, यदि हम किसी स्थान पर हरे वृक्ष देखते हैं और वहां पक्षियों की आवाज सुनते हैं, तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर पानी होने का अनुमान हो सकता है। लेकिन यह केवल संभाव्यता है, न कि निश्चित ज्ञान।
चार्वाक दर्शन में शब्द का प्रयोग भी प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर ही समझा जाता है। वेदों के वचन, जो अदृष्ट और अश्रुत विषयों का वर्णन करते हैं, उन्हें अप्रामाणिक और संदिग्ध माना जाता है।
चार्वाक का आचारमीमांसा
चार्वाक दर्शन का आचारमीमांसा जीवन की भौतिक सुख-साधना पर आधारित है। उनका मत है कि मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से केवल अर्थ और काम ही वास्तविक और उपयोगी पुरुषार्थ हैं।
चार्वाकों के अनुसार, धर्म और यज्ञ जैसे कार्य केवल शरीर को कष्ट पहुँचाने और संसाधनों का व्यर्थ प्रयोग करने के लिए हैं। इसलिए, जो कार्य मनुष्य को सुख और आनन्द प्रदान करे, वही वास्तविक धर्म है। यह दृष्टिकोण जीवन की सुखवादी और यथार्थवादी व्याख्या प्रस्तुत करता है।
चार्वाक दर्शन और बृहस्पति
चार्वाक दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक बृहस्पति माने जाते हैं। हालांकि, भारतीय साहित्य में बृहस्पति का उल्लेख कई रूपों में मिलता है—जैसे आंगिरस बृहस्पति, लौक्य बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति आदि। चार्वाक दर्शन के सन्दर्भ में बृहस्पति वेद विरोधी और तर्कसिद्ध उपदेशक माने जाते हैं।
कुछ विद्वानों के अनुसार, चार्वाक दर्शन और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रचनाकार बृहस्पति एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। इसके अनुसार चार्वाक दर्शन का उद्देश्य लौकिक इच्छाओं और भौतिक सुख की प्राप्ति था।
चार्वाक और लोकायत दर्शन
चार्वाक दर्शन को सरल भाषा में लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। इसका अर्थ है—वह दर्शन जो सामान्य जनता के लिए सहज और प्रिय हो। जीवन के प्रत्येक पहलू में चार्वाक दृष्टिकोण स्पष्ट है—भौतिक सुख और प्रत्यक्ष अनुभव को सर्वोच्च माना गया है।
इस दर्शन का मूल संदेश यह है कि जीवन में खाने-पीने, आनंद, सुख और भौतिक तृप्ति का पालन करना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। यह दृष्टिकोण समाज के सर्वसामान्य अनुभवों और व्यवहार से भी पूरी तरह मेल खाता है।
चार्वाक दर्शन ने भारतीय दर्शनशास्त्र में नास्तिक और भौतिकवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। यह प्रत्यक्ष अनुभव और भौतिक सुख को सर्वोच्च मानता है, ईश्वर, आत्मा और परलोक जैसी अवधारणाओं को अस्वीकार करता है। जीवन को यथार्थ और अनुभवजन्य दृष्टि से समझना ही इसका मूल संदेश है।