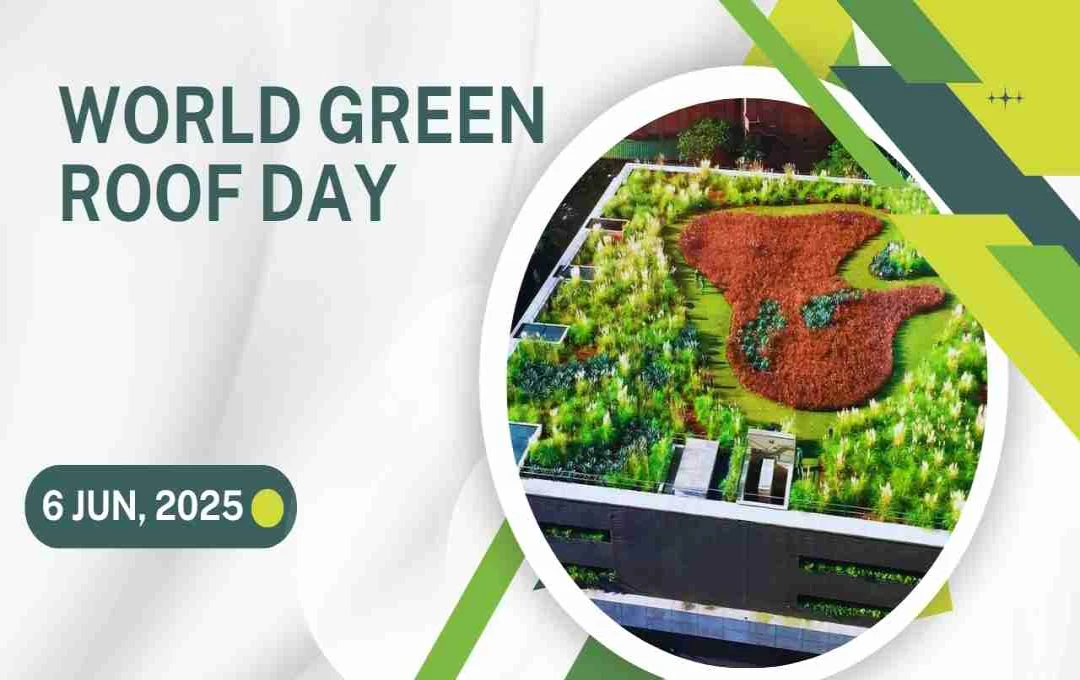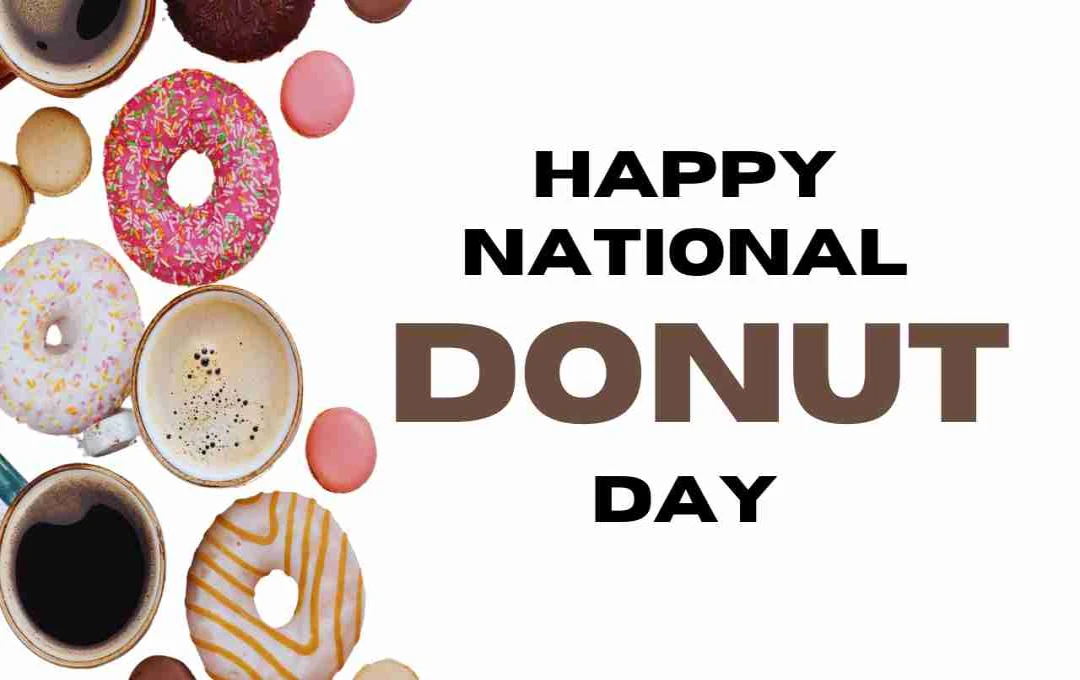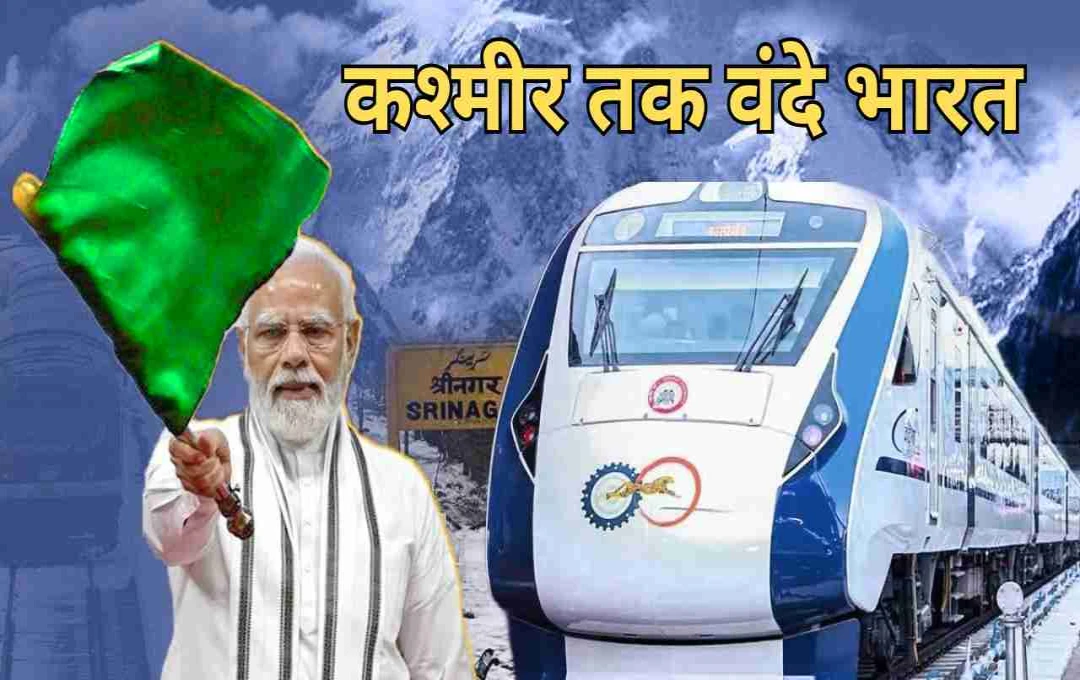विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का निर्णय यूनेस्को ने अपने 36वें सम्मेलन के दौरान 3 नवंबर 2011 को लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो के महत्व को उजागर करना और लोगों को इसके उपयोग के प्रति जागरूक करना है। रेडियो, संचार का एक सशक्त माध्यम है, जो न केवल जानकारी प्रसारित करता है, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन और आपातकालीन परिस्थितियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं।
यह दिन दुनियाभर में रेडियो प्रसारणकर्ताओं, पत्रकारों और श्रोताओं को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है ताकि वे रेडियो की शक्ति और इसकी सामाजिक भूमिका को पहचान सकें।
विश्व रेडियो दिवस का इतिहास

विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 2011 में अपनी जनरल कॉन्फ्रेंस में इस दिन को मान्यता दी, और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। 13 फरवरी 1946 को यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल द्वारा संयुक्त राष्ट्र रेडियो और संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण सेवा की स्थापना की गई थी। इसी कारण 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में चुना गया।
रेडियो का महत्व और उद्देश्य
विश्व रेडियो दिवस का मुख्य उद्देश्य रेडियो की शक्ति और उसकी सामाजिक भूमिका को पहचानना और इसे एक प्रभावी संचार माध्यम के रूप में बढ़ावा देना है। यह दिन रेडियो स्टेशनों, प्रसारकों और श्रोताओं को एक साथ लाने का अवसर प्रदान करता है, ताकि वे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझ सकें। यूनेस्को रेडियो स्टेशनों को विभिन्न सामग्री जैसे कि समाचार, विशेष शो, ऑडियो कार्यक्रम आदि प्रदान करता हैं।
यह सामग्री कॉपीराइट-मुक्त होती है, जिससे सभी रेडियो स्टेशन इसे आसानी से उपयोग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और उनकी जानकारी बढ़ाना है। इसकी स्थापना और प्रसार में कई संगठन शामिल थे, जिनमें शामिल हैं।
*सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक प्रसारक
* संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, फंड और कार्यक्रम
* गैर सरकारी संगठन (NGOs)
* शिक्षाविद, फाउंडेशन और विकास एजेंसियां
कैसे मनाया जाता हैं विश्व रेडियो दिवस?

1. रेडियो स्टेशनों द्वारा विशेष प्रसारण
* रेडियो स्टेशन इस दिन विशेष कार्यक्रम, इंटरव्यू, डिबेट और संगीत कार्यक्रम प्रसारित करते हैं।
* ऐतिहासिक रेडियो घटनाओं, प्रसिद्ध रेडियो हस्तियों और रेडियो की ताकत पर चर्चा होती है।
* कुछ स्टेशन इस दिन लाइव कॉलर से बातचीत कर उनके अनुभव साझा करते हैं।
2. जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं
* रेडियो उद्योग से जुड़े पेशेवरों द्वारा सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं।
* स्कूलों, कॉलेजों और मीडिया संस्थानों में रेडियो के प्रभाव और उसकी भूमिका पर चर्चाएं होती हैं।
* स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों द्वारा रेडियो की भूमिका पर वेबिनार और ऑनलाइन चर्चाएं की जाती हैं।
3. सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभियान
* लोग #WorldRadioDay और #RadioForPeace जैसे हैशटैग के साथ रेडियो से जुड़ी अपनी यादें और अनुभव साझा करते हैं।
* रेडियो स्टेशनों और मीडिया हाउस द्वारा वीडियो, ऑडियो क्लिप और इन्फोग्राफिक्स जारी किए जाते हैं, जिनमें रेडियो के इतिहास और योगदान को दर्शाया जाता है।
4. स्थानीय और सामुदायिक कार्यक्रम

* कई जगहों पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करने और लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करते हैं।
* गांवों और छोटे कस्बों में रेडियो के उपयोग और उसकी शक्ति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाते हैं।
5. सम्मान और पुरस्कार वितरण
* रेडियो इंडस्ट्री में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को यूनेस्को और अन्य मीडिया संगठनों द्वारा सम्मानित किया जाता है।
* रेडियो जॉकी (RJ), ब्रॉडकास्टर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।