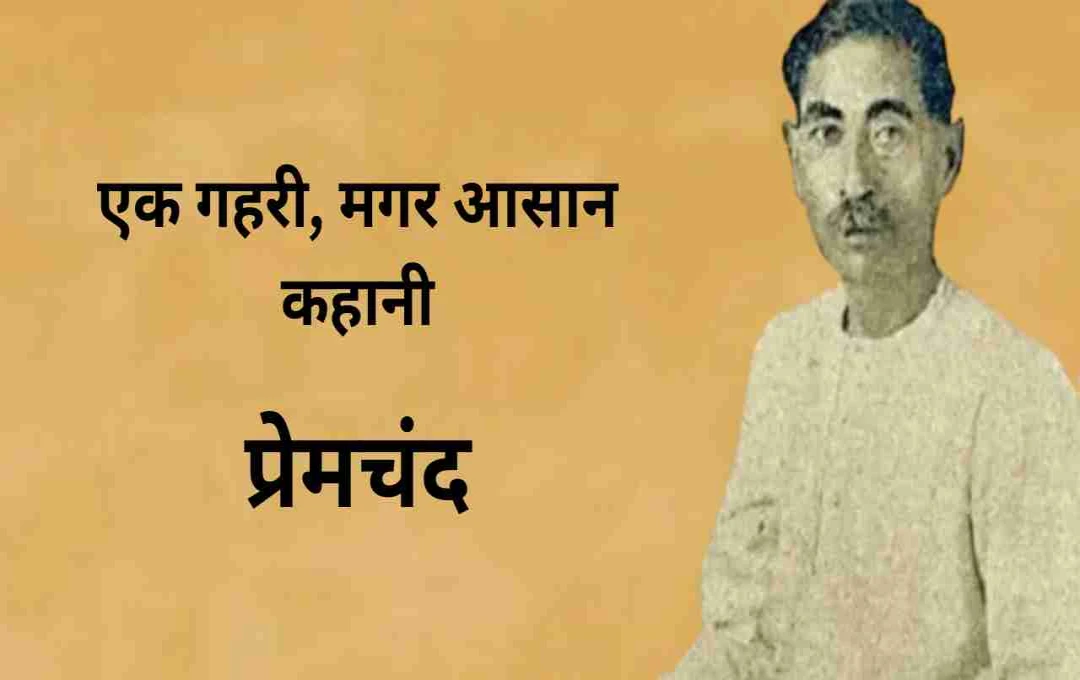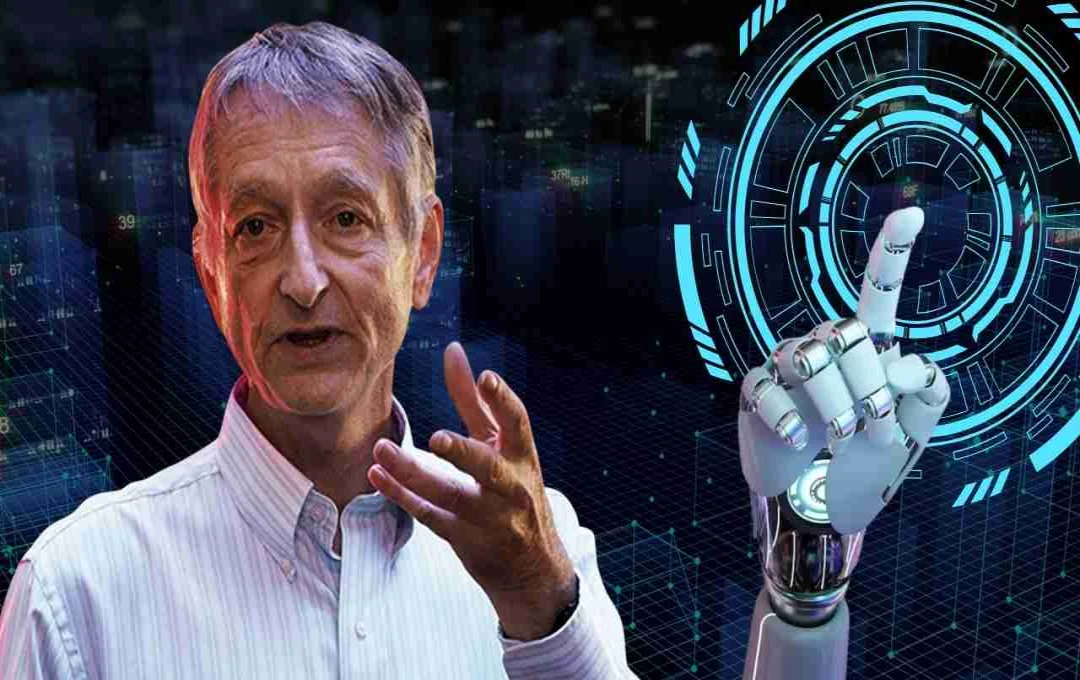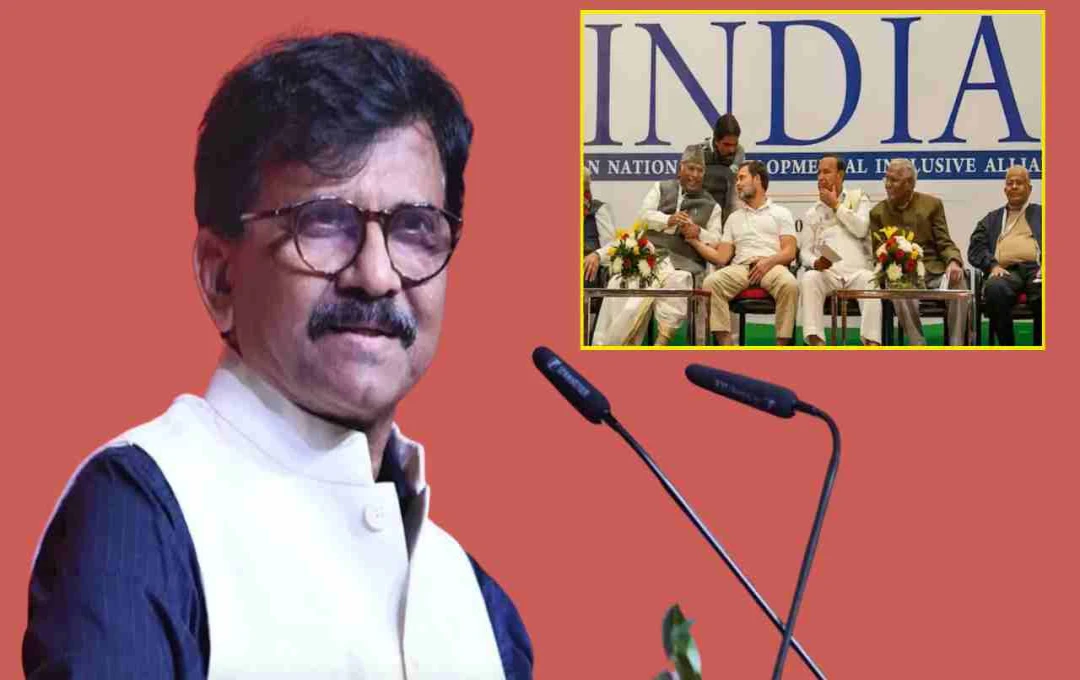1856 का समय था। भारत की आज़ादी से पहले का वह दौर, जब अंग्रेज धीरे-धीरे देश के विभिन्न हिस्सों पर अपना नियंत्रण मजबूत करते जा रहे थे। उस समय अवध एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से संपन्न राज्य था, जिसकी राजधानी लखनऊ थी। वहां के नवाब वाजिद अली शाह, संगीत, नृत्य और कविता के शौकीन थे, लेकिन राजनीति से उनका कोई खास लेना-देना नहीं था।
इसी लखनऊ शहर में दो ऐसे नवाब भी रहते थे – मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों ही ऊँचे खानदानों के रईस थे। धन-दौलत, नौकर-चाकर, बड़ा सा घर, सब कुछ था उनके पास। लेकिन उनकी असली पहचान थी – शतरंज का दीवानापन।
शतरंज: खेल से बढ़कर जुनून
मिर्जा और मीर के लिए शतरंज केवल एक खेल नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। सुबह की शुरुआत शतरंज से होती, दोपहर और शाम उसी के नाम, और रात को भी मोमबत्ती या दीपक की रोशनी में गोटियाँ चलती रहतीं।
इनकी यह दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अपने घर, बीवी-बच्चों, यहां तक कि समाज की परवाह करना छोड़ दिया था। मिर्जा की पत्नी, जो समझदार और शालीन महिला थीं, कई बार उन्हें समझाने की कोशिश करतीं 'हुज़ूर, ये खेल कब तक चलेगा? कभी हमारे साथ भी थोड़ा वक़्त बिताइए।' लेकिन मिर्जा हंसकर बात टाल देते 'बेगम, ये जंग है, अभी सैनिकों को संभालना है।'
उधर मीर की पत्नी भी परेशान हो चुकी थीं। वो कहतीं – 'इनके लिए तो मैं नहीं, शतरंज ही बीवी है।' जब हद हो गई तो दोनों की पत्नियाँ अपने-अपने मायके चली गईं। मगर मिर्जा और मीर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा – उनके लिए तो बस शतरंज की बाजी ही सबसे बड़ी थी।
लखनऊ का हाल और नवाब की सुस्ती
इधर, लखनऊ की गद्दी पर नवाब वाजिद अली शाह का राज था। लेकिन वे एक कला प्रेमी शासक थे, जो शायरी, नृत्य, और संगीत में डूबे रहते थे। उनके दरबार में कव्वालियाँ होती थीं, मुशायरे होते थे और वे सभी को खुश होकर इनाम देते थे। उन्हें शासन और राजनीति में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी।
अंग्रेजों को इस कमजोरी का एहसास था। वे समझ चुके थे कि इस नवाब को हटाना बहुत आसान होगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई और चुपचाप अवध को अपने कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी। एक दिन नवाब साहब को अंग्रेजी सरकार की ओर से पत्र मिला – 'आपका शासन समाप्त किया जा रहा है, कृपया दिल्ली या कलकत्ता चले जाइए।'
लखनऊ में चारों तरफ उथल-पुथल मच गई। महलों में हलचल थी, सड़कों पर सैनिक दौड़ रहे थे, तोपों की आवाजें गूंज रही थीं – लेकिन मिर्जा और मीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।
जब लखनऊ जल रहा था, दो नवाब खेल रहे थे शतरंज
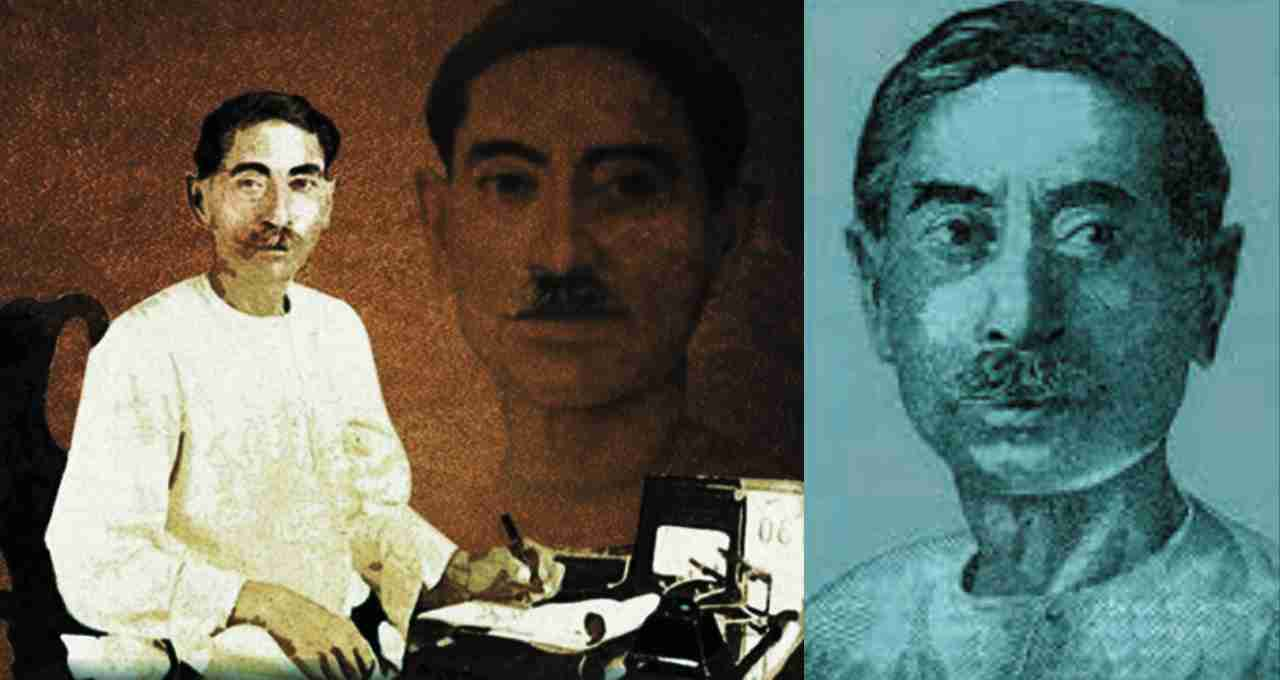
जहां एक ओर लखनऊ पर अंग्रेज कब्ज़ा कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये दोनों नवाब किसी पुराने खंडहर में शतरंज की बाजी में डूबे थे। उन्होंने शहर की हलचल से बचने के लिए एक शांत और वीरान जगह तलाश ली थी – ताकि कोई उन्हें परेशान न करे।
वो कहते – 'अंग्रेज आएं या जाएं, हमें क्या लेना? हमारी बादशाहत तो शतरंज की चौसर पर कायम है।' उनका सारा ध्यान केवल इस बात पर था कि अगली चाल कौन-सी चले जिससे वह जीत सकें।
लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकी। एक दिन खेलते-खेलते बाज़ी में झगड़ा हो गया। मिर्जा ने मीर पर आरोप लगाया कि उन्होंने गोटियाँ गलत चलाई हैं। 'तुमने प्यादे को दो घर आगे बढ़ा दिया, जबकि नियम के हिसाब से एक घर ही चल सकते हो!'
मीर तिलमिला उठे – 'तुम मुझ पर बेईमानी का इल्ज़ाम लगाते हो?' बात-बात में गुस्सा बढ़ गया और दोनों ने तलवारें खींच लीं।
दोस्ती का युद्ध
अब तक जो खेल के साथी थे, वे एक-दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। तलवारें चमकने लगीं और माहौल गर्म हो गया। मिर्जा बोले – 'अगर जीतने के लिए दोस्ती तोड़नी पड़े, तो मैं हार ही बेहतर समझता हूं।'
मीर भी पीछे नहीं हटे – 'तो फिर तलवार से फैसला हो!'
लेकिन जैसे ही तलवारें आमने-सामने आईं, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे ठहर गए, कुछ पल चुप रहे, और फिर मीर बोले – “क्या हम इतने गिर चुके हैं कि एक खेल के लिए दोस्ती और इंसानियत भी भूल जाएं?”
दोनों की आंखें भर आईं। उन्होंने तलवारें नीचे कर दीं और एक-दूसरे से माफी मांगी।
पछतावे का पल
अब तक जब वे आंखें खोल चुके थे, तब तक सब कुछ बदल चुका था। खंडहर के बाहर अंग्रेजी सैनिकों की आवाजें आ रही थीं। लखनऊ अब अंग्रेजी राज के अधीन हो चुका था। मिर्जा और मीर को अपने गुनाह का एहसास हुआ – कि उन्होंने शतरंज के चक्कर में अपने परिवार, समाज और देश की परवाह नहीं की। जब वक्त उन्हें जिम्मेदारी निभाने को कह रहा था, वे अपने ही खेल में उलझे हुए थे।
कहानी की सीख
‘शतरंज के खिलाड़ी’ केवल दो नवाबों की कहानी नहीं है। यह उस समय का चित्र है, जब पूरा देश संकट में था, और समाज के उच्च वर्ग के कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर केवल अपने शौकों में मस्त थे। प्रेमचंद ने इस कहानी के ज़रिए एक तीखा सवाल उठाया है – क्या जब देश और समाज किसी मुसीबत में हो, तब भी हमें केवल अपने शौक और आराम की चिंता करनी चाहिए?
यह कहानी यह भी दिखाती है कि कैसे एक साधारण खेल, जब आदत या ज़िद बन जाए, तो वह रिश्तों को तोड़ सकता है, इंसानियत भुला सकता है, और सबसे बढ़कर – समय की पुकार को अनसुना कर सकता है। प्रेमचंद की ‘शतरंज के खिलाड़ी’ एक सरल, मगर गहराई से भरी कहानी है। यह हमें हँसाती भी है, सोचने पर भी मजबूर करती है और एक ऐसी सीख देती है जिसे आज के हर इंसान को जानना चाहिए।