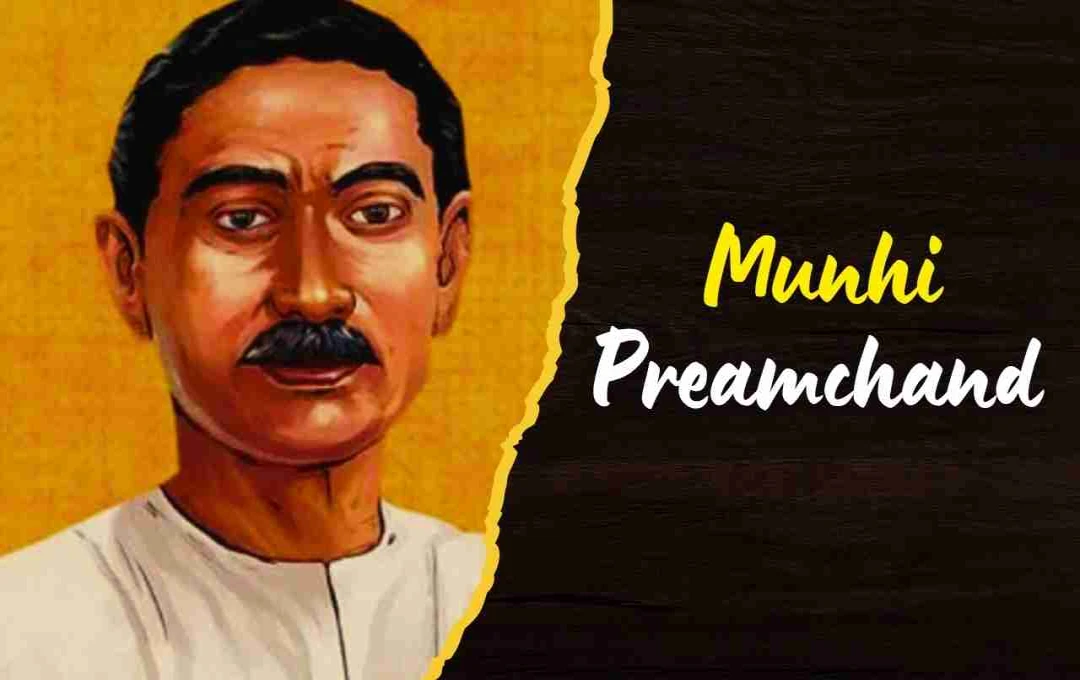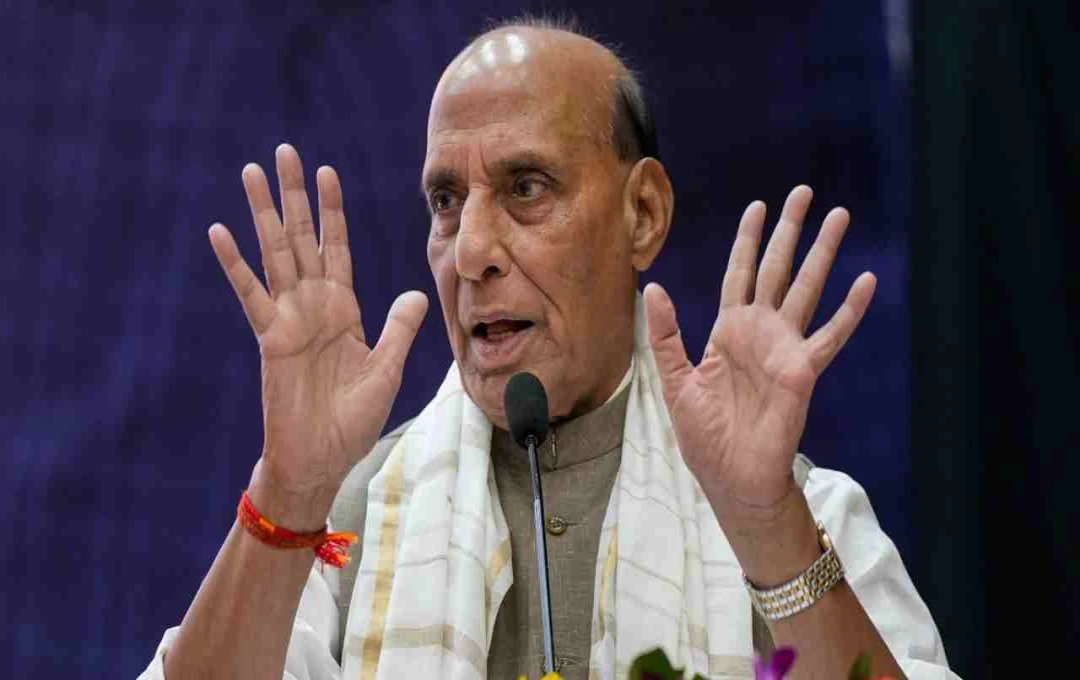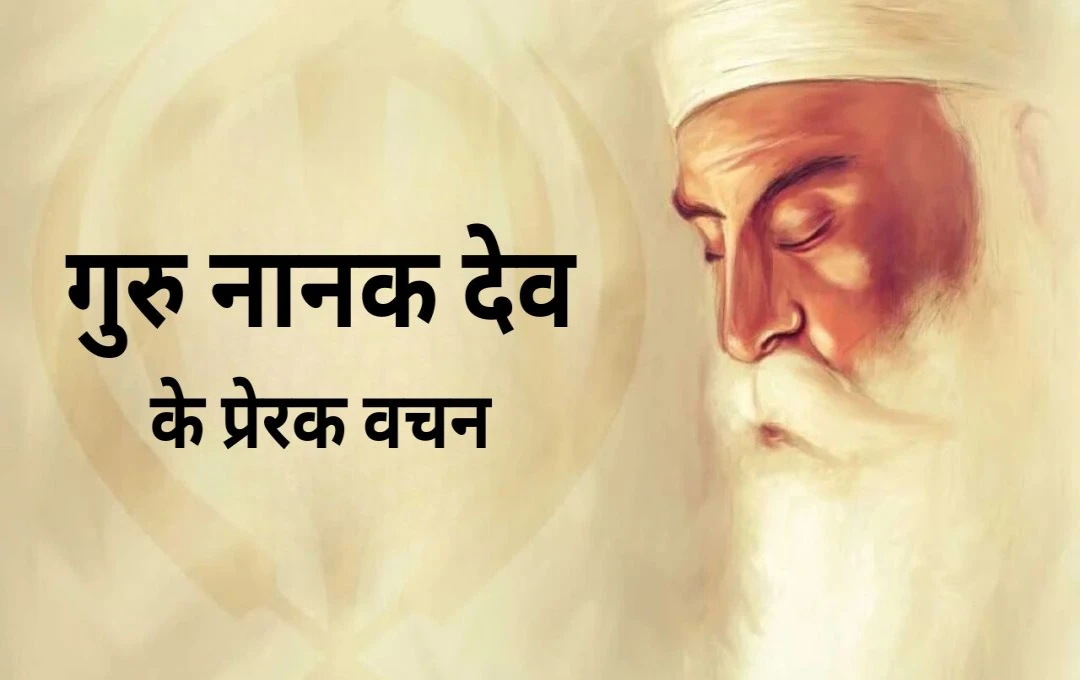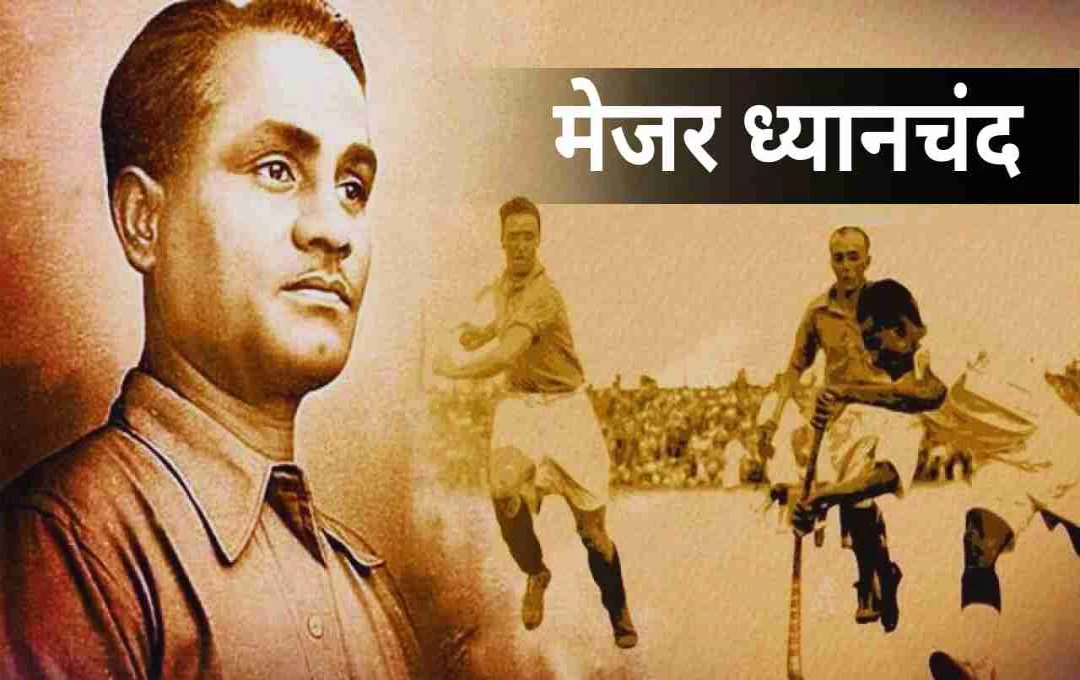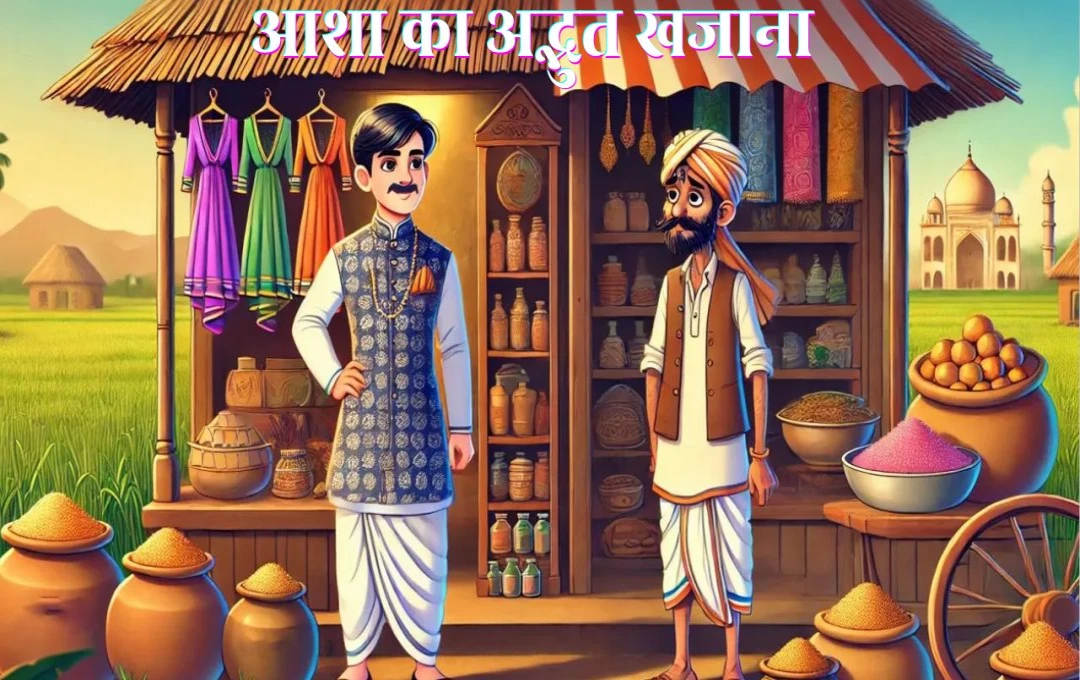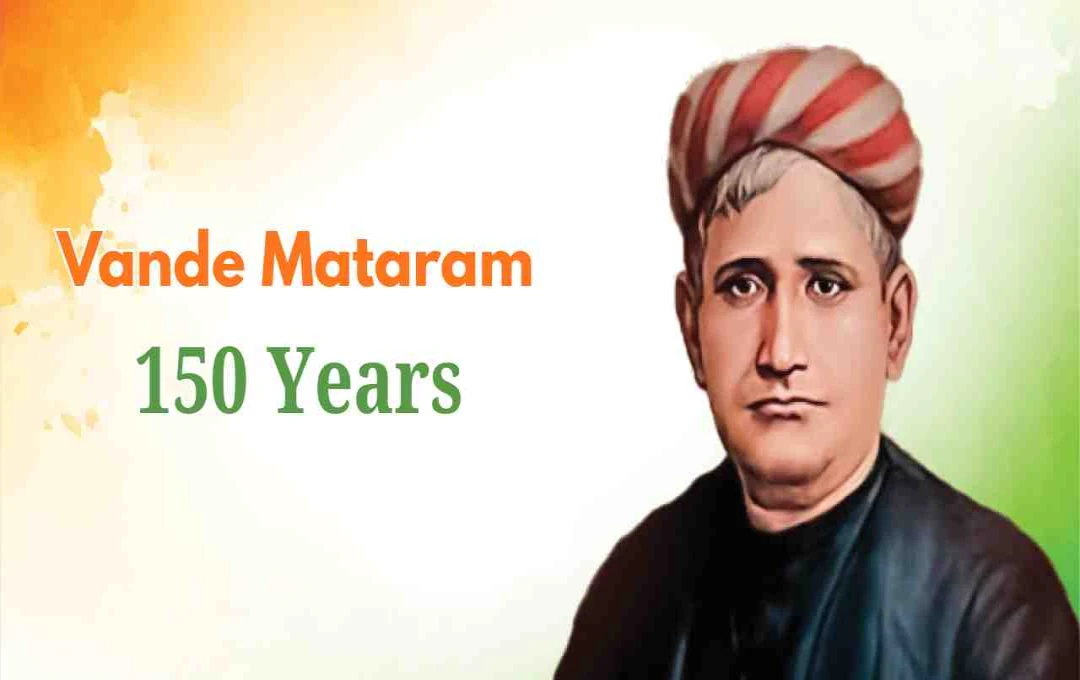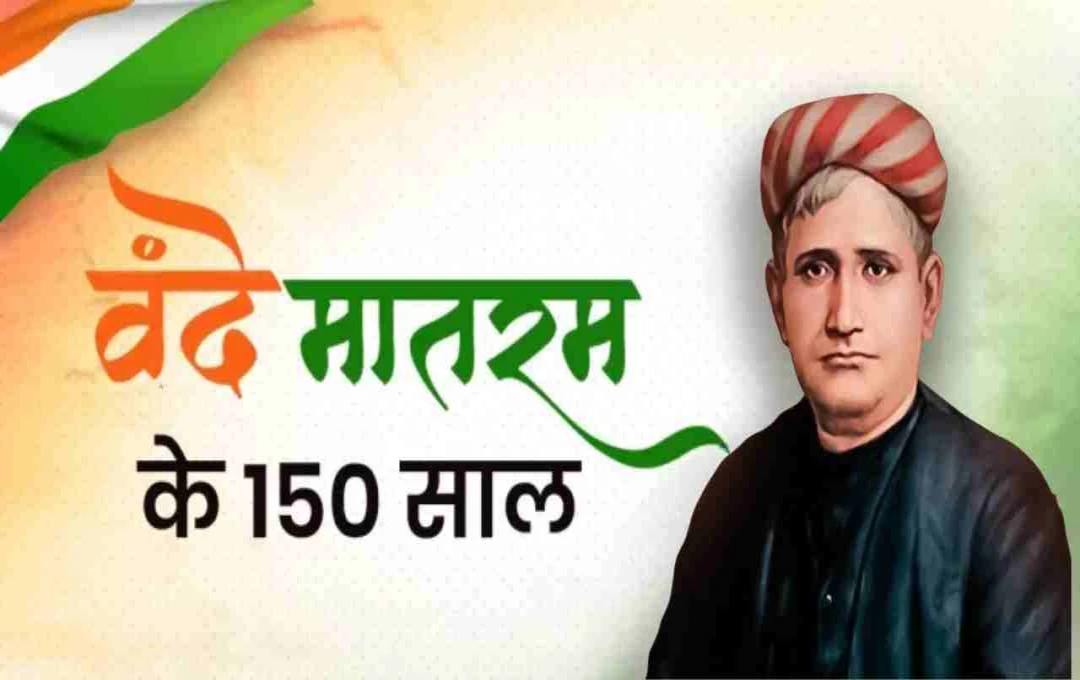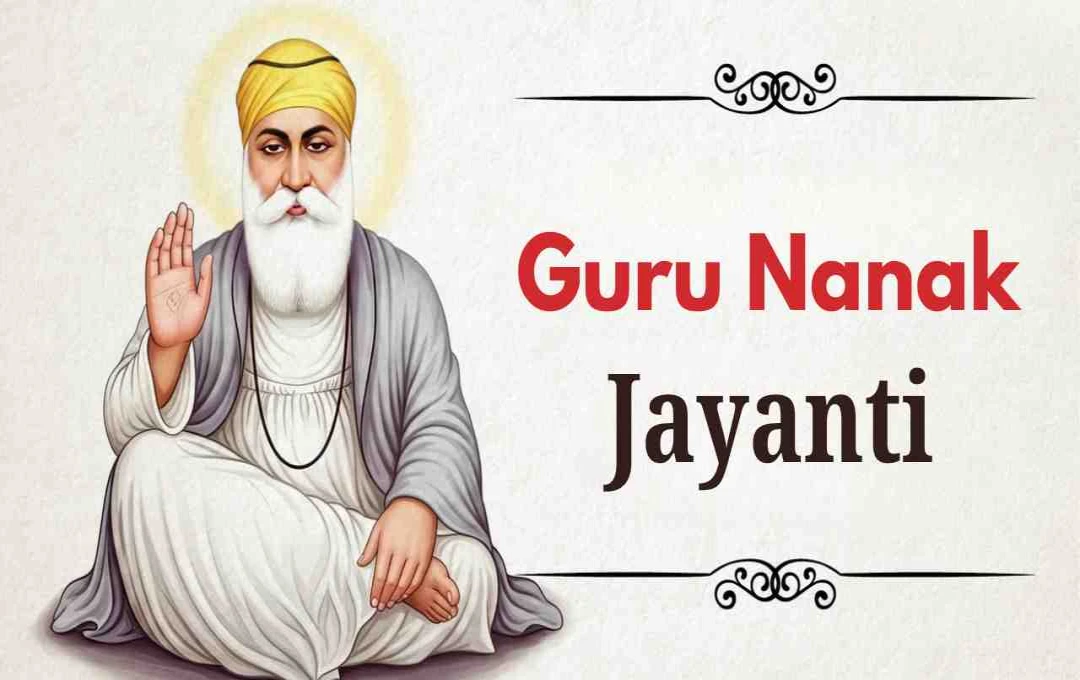मुंशी प्रेमचंद का नाम आते ही मन में एक ऐसी छवि बनती है जो समाज के सबसे साधारण और पीड़ित वर्ग की बात करता है। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही गांव में हुआ था। वे न सिर्फ हिंदी बल्कि उर्दू साहित्य के भी महान लेखक माने जाते हैं। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, लेकिन वे साहित्य की दुनिया में ‘प्रेमचंद’ के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने लेखन से समाज के गहरे दर्द, असमानता और शोषण को जिस सजीव रूप में प्रस्तुत किया, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
कहानियों में ग्रामीण भारत की सच्चाई
प्रेमचंद की कहानियों का मुख्य फोकस गांव, किसान, मजदूर, और निम्न वर्ग होता था। उन्होंने अपने पात्रों को बेहद साधारण लेकिन गहराई से संवेदनशील बनाया। उनकी कहानियां उस समय के भारत की तस्वीर पेश करती हैं जिसमें गरीबी, सामाजिक भेदभाव और धार्मिक रूढ़ियों का बोलबाला था। उदाहरण के लिए, कहानी ‘पूस की रात’ में हल्कू नामक किसान की गरीबी और बेबसी को इतने संवेदनशील तरीके से दर्शाया गया है कि पाठक का दिल भर आता है। रात को खेत की रखवाली करते समय जब हल्कू ठंड से कांप रहा होता है और आग नहीं जला सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं — यह दृश्य आज भी पाठकों को झकझोर देता है।
यथार्थवाद का अद्भुत चित्रण
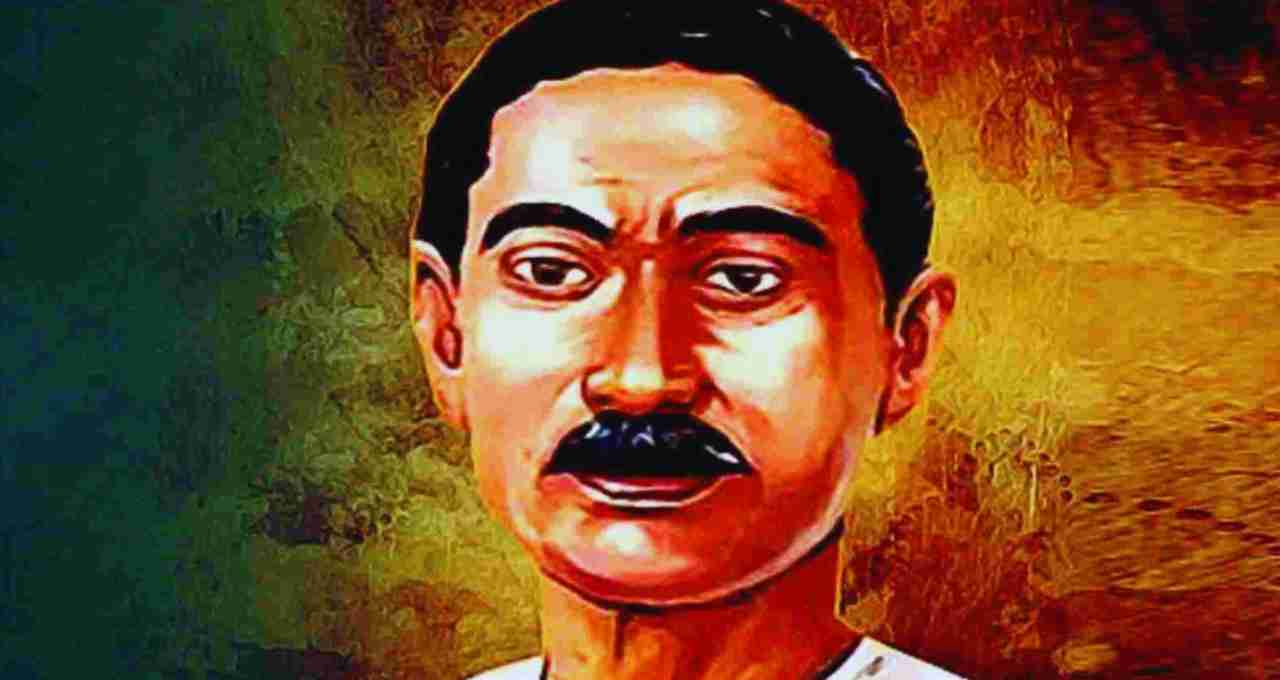
प्रेमचंद की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी यथार्थवादी दृष्टि। वे किसी विषय को अलंकारिक ढंग से नहीं, बल्कि उसकी असलियत के साथ प्रस्तुत करते थे। चाहे वह ‘कफन’ जैसी मार्मिक कहानी हो, जिसमें गरीबी इतनी चरम पर है कि बेटे और बहू की मृत्यु के बाद भी बाप और बेटा उसके नाम पर शराब पी जाते हैं — प्रेमचंद ऐसे कड़वे सच को सामने लाने में कभी हिचकिचाए नहीं। प्रेमचंद ने दिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए पहले उसकी सच्चाई को समझना और स्वीकारना जरूरी है।
नारी की स्थिति और संघर्ष
प्रेमचंद की कहानियों में महिलाओं की स्थिति भी बार-बार उभरकर सामने आती है। उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, शोषण और उनकी चुप आवाज़ को अपनी कहानियों में जगह दी। ‘सेवासदन’ और ‘गबन’ जैसे उपन्यासों में स्त्रियों के जीवन और उनके आत्मसम्मान की तलाश को बहुत खूबसूरती और सच्चाई से पेश किया गया है। उन्होंने महिलाओं को सिर्फ पीड़िता के रूप में नहीं, बल्कि संघर्षशील और स्वाभिमानी रूप में भी दिखाया।
सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा
प्रेमचंद का साहित्य केवल समाज की बुराइयों का आईना नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की प्रेरणा भी देता था। वे चाहते थे कि शोषित और गरीब लोग अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उनकी कहानियों में यह स्पष्ट झलकता है कि बदलाव संभव है — अगर लोग संगठित हों, शिक्षित हों और जागरूक बनें। ‘ईदगाह’ कहानी में हामिद की दादी के लिए चिमटा खरीदने की मासूम भावना एक तरफ जहां त्याग और सच्चे प्रेम को दर्शाती है, वहीं दूसरी तरफ समाज की बुनियादी ज़रूरतों और इच्छाओं की कमी की ओर इशारा करती है।
भाषा और शैली की सरलता
प्रेमचंद की भाषा आम जनमानस की भाषा थी। वे संवादों और सरल शब्दों के माध्यम से बड़े से बड़े विचारों को इस तरह प्रस्तुत करते थे कि हर पाठक उससे जुड़ सके। उन्होंने संस्कृतनिष्ठ हिंदी या फारसीभाषा से दूरी बनाकर जनभाषा को साहित्य की भाषा बनाया। उनकी शैली में न नाटकीयता होती थी और न ही भावनात्मक अतिरेक — बस एक सहज, सच्ची, जीवन के करीब कहानी होती थी जो सीधे दिल में उतर जाती है।
कालजयी कहानियां: जो आज भी उतनी ही जीवंत हैं
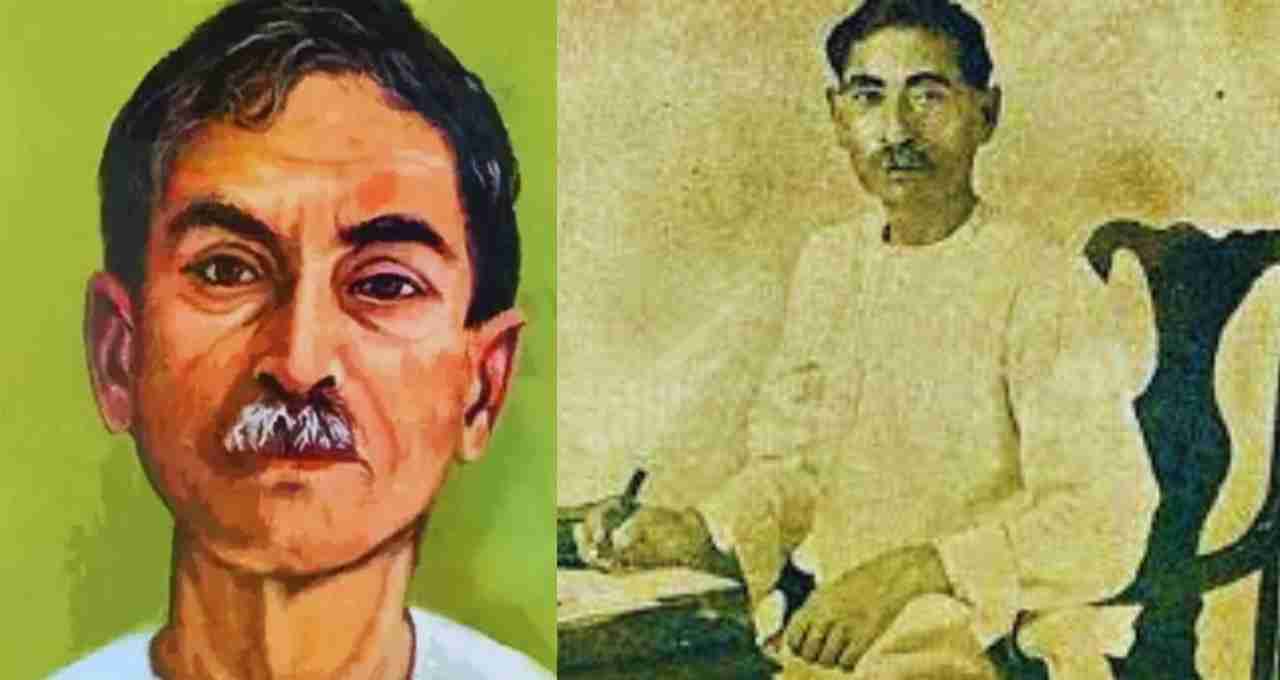
मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 से अधिक कहानियां और 12 उपन्यास लिखे। उनकी कुछ कहानियां जो आज भी सबसे ज्यादा पढ़ी और सराही जाती हैं, वे हैं:
- कफन
- ईदगाह
- पूस की रात
- नमक का दरोगा
- बड़े घर की बेटी
- सत्य का प्रयोग
हर कहानी समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करती है — चाहे वह जात-पात हो, अमीरी-गरीबी का फर्क हो या नारी शोषण।
प्रेमचंद की विरासत: आज भी उतनी ही प्रभावशाली
प्रेमचंद की कहानियां आज भी स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं, नाटकों और फिल्मों का आधार बनती हैं और साहित्यिक शोध का केंद्र हैं। उनकी लेखनी समय की सीमाओं को पार कर चुकी है। उन्होंने जिस ईमानदारी, संवेदनशीलता और गहराई के साथ लिखना सिखाया — वह आज के लेखकों के लिए भी आदर्श है। उन्होंने बताया कि साहित्य केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का आईना और सुधार का उपकरण भी हो सकता है।
मुंशी प्रेमचंद सिर्फ एक लेखक नहीं थे, बल्कि एक सामाजिक सुधारक, विचारक, और जनमानस के प्रतिनिधि थे। उनकी कहानियों में हमें न केवल अतीत की झलक मिलती है, बल्कि आज के समाज की भी सचाई दिखाई देती है। उनके साहित्य से यह सीख मिलती है कि जब तक समाज में अन्याय, भेदभाव और पीड़ा है — तब तक प्रेमचंद की लेखनी प्रासंगिक रहेगी।